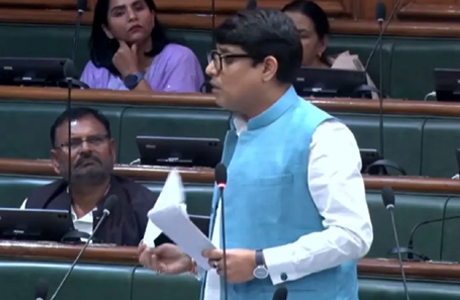पंचायतों का तालिबानी फैसला – हुक्का पानी बंद
बच्चों ने प्रेम विवाह कर लिया तो परिवार का हुक्का पानी बंद. किसी ने अंध-विश्वास और दकियानूसी परम्पराओं का विरोध किया तो उसका भी हुक्का पानी बंद. अकसर पंचायतें पहले दंड लगाती हैं और जब पीड़ित दंड की राशि नहीं दे पाता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है. यह भी एक तरह की ब्लैकमेलिंग है जिसे समाज ने स्वीकार कर लिया है. हुक्का पानी खत्म करने की भी अपनी रेट लिस्ट होती है. अपराध के आकार प्रकार के आधार पर दण्ड लगाया जाता है. एक बार हुक्का पानी बंद होने पर दण्ड की राशि बढ़ जाती है. हुक्का पानी दोबारा शुरू करवाने के लिए परिवार को या तो अपने खेत बेचने पड़ते हैं या फिर कर्ज लेकर पंचायत का पेट भरना पड़ता है. अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति के डॉ दिनेश मिश्रा के अनुसार यह राशि छत्तीसगढ़ में 15 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक जाती है. देश में कभी पंचों को परमेश्वर की संज्ञा दी गई थी. इन्हीं पंच और सरपंचों को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में व्यापक अधिकार दिये गये. कालांतर में यही पंचायतें राजनैतिक दलों की नर्सरी बनकर सामने आईं. पंचायतों के पास सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के असीमित अधिकार हैं. उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पाई जाने वाली खाप पंचायतें तो काफी बदनाम हैं. देश की अधिकांश पंचायतें प्रेम संबंधों के खिलाफ हैं. कहीं प्रेमी-प्रेमिका को बांध कर बेदम पीटा जाता है तो कहीं उन्हें साथ-साथ फांसी पर लटका दिया जाता है. कहीं युवती को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया जाता है तो कहीं उसके सार्वजनिक सामूहिक बलात्कार का फैसला सुना दिया जाता है. फूलन देवी भी एक ऐसी ही पीड़ित थी जिसपर गांव के रसूखदारों ने अनगिनत जुल्म ढाए. जब फूलन को कहीं से न्याय नहीं मिला तो उसने बीहड़ों में जाकर बंदूक उठा लिया. 14 फरवरी, 1981 को फूलन ने बेहमई गांव में 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी. बहरहाल, यहां बात हुक्का पानी बंद करने की हो रही थी. यह एक ऐसी सजा है जो हमारी अदालतों द्वारा दी जाने वाली किसी भी सजा से ज्यादा कठोर है. इसमें परिवार का गांव में रहना मुश्किल कर दिया जाता है. न कोई उससे बोलता है, न बुलाता है. जिसका हुक्का पानी बंद हो, उसके साथ किसी भी तरह का कारोबारी संबंध या रिश्तेदारी नहीं निभाई जा सकती. पीड़ित परिवार गांव के किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो सकता. गांव की दुकानों से सौदा नहीं खरीद सकता. गांव के सार्वजनिक तालाब और कुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता. परिवार को घुट-घुट कर अकेले जीना होता है. उनके बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव होता है. कई बार तो उनके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी जाती है. यह उनसे उनके नागरिक होने का अधिकार छीन लेने जैसा है. इसलिए अब इसे चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग उठी है.
Diplay pic courtesy Jagran.com